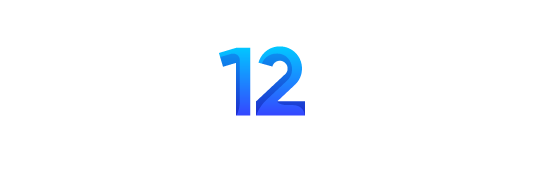अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें कि भारतीय साहित्य में कौन सी अवधारणाएं पुरानी पड़ रही हैं और कौन सी नई अवधाराणाएं आकार ले रही हैं तो हम ‘बहुजन’ अवधारणा को अंकुरित होते महसूस करते हैं। इस आलेख में हम इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्यों हो रहा है, इसका इतिहास क्या है, कौन सी शक्तियां इसके विरोध में हैं। साथ ही हम इसमें इसकी संभावित सैद्धांतिकी पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे।
बहुजन साहित्य की सुगबुहाट
पिछले कुछ समय से भारत के विभिन्न हिस्सों में साहित्य पर केंद्रित ऐसे अनेक कार्यक्रम होने लगे हैं, जिनमें किसी-न-किसी रूप में ‘बहुजन साहित्य’ शब्द-बंध का प्रयोग किया जा रहा है। सन् 2017 में जयपुर में ‘बहुजन साहित्य महोत्सव’ मनाया गया, जिसमें ‘समकालीन साहित्य में बहुजन चेतना’ पर विस्तार से चर्चा हुई थी। सन् 2018 में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ‘बहुजन साहित्य संघ’ की स्थापना की गयी और ‘बहुजन साहित्य की अवधारणा और सौन्दर्यबोध’ समेत बहुजन साहित्य से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम हुए। हाल ही में बने ‘जन लेखक संघ’ के तत्त्वावधान में इसी 5 जून, 2022 को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में ‘बहुजन साहित्य:दशा और दिशा’ विषय पर गोष्ठी हुई, जिसमें कई हिंदी-भाषी राज्यों के लेखकों ने भाग लिया। ऐसे दर्जनों कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लो भागीदारी कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को गूगल अथवा फेसबुक के सर्च इंजन में आसानी से तालाशा जा सकता है। हिन्दी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और तमिल में भी बहुजन साहित्य पर केंद्रित आयोजनों के होने की सूचनाएँ मिल रही हैं। तेलांगना में बहुजन साहित्य अकादमी सक्रिय है, जिसका एक बड़ा आयोजन पिछले दिनों दिल्ली में हुआ था। इस प्रकार केरल में बहुजन साहित्य अकादमी स्थापित हुई है।
इन आयोजनों के अलावा एक और परिवर्तन दिख रहा है। मसलन, डॉ. आम्बेडकर के नाम से जुड़ा इलाहाबाद का एक संगठन ‘वर्तमान परिदृश्य में हिन्दू कोड बिल : जाति और पितृसत्ता’ विषय पर सेमिनार आयोजित कर रहा है। इसके आमंत्रण-पत्र में बताया गया है कि यह ‘बहुजन महिला साहित्यकारों’ का महासम्मेलन है। कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ताओं में जिन महिलाओं के नाम हैं, उन्हें ‘वरिष्ठ बहुजन साहित्यकार’ कहकर सम्बोधित किया है। ये वे महिला साहित्यकार हैं, जो अनुसूचित जाति के परिवारों में पैदा हुई हैं तथा अब तक उनका परिचय ‘दलित साहित्यकार’ के रूप में हुआ करता था।
साहित्य, संस्कृति को देखने का यह नया नज़रिया क्यों विकसित हो रहा है? ये आयोजन बहुजन अवधारणा के तहत होने वाले दलित,आदिवासी, मध्यवर्ती जातियों; जिन्हें भारतीय संविधान में ओबीसी कहा गया है; तथा हमारे विमर्श के दायरे से अलक्षित रहे अन्य सामाजिक समूहों की संस्कृति और साहित्यिक अभिव्यक्तियों में व्यक्त मूल्यों के साझेपन को अपने-अपने तरीक़े से चिह्नित कर रहे हैं। साथ ही इनमें सामाजिक स्तर पर द्विजवाद से संघर्ष के मुद्दों के साझेपन की तलाश की जा रही है। इन आयोजनों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण यह भी है कि इन कोशिशों के पीछे कोई सुव्यवस्थित संगठन नहीं है, बल्कि यह स्वयमेव हो रहा है।
अतीत और भविष्य
इस विषय पर आगे बात करने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी होंगी। पहली यह कि इस समय भारतीय साहित्य में दो ही मान्य धाराएं हैं, एक प्रगतिशील धारा और दूसरी दलित धारा। इन दोनों साहित्यिक आन्दोलनों ने स्वर्णिम युग देखे हैं तथा भारतीय साहित्य की रीति-नीति को बदलने में क्रान्तिकारी भूमिका निभायी है। ‘बहुजन अवधारणा’ अभी दृश्य-पटल पर उस रूप में मौजूद नहीं है कि हम उसे साफ-साफ देख सकें।
यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रगतिशील साहित्य आन्दोलन और दलित साहित्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जनपक्षधर राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान करते रहे हैं। इनकी असफलता के फलाफल में भारतीय राजनीति में अभिव्यक्ति की आज़ादी का विरोधी, नागरिकों को अपनी प्रजा समझने वाला, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिंसक विरोध करने वाला, विज्ञान और तकनीक की नई प्रविधियों को नागरिकों को ग़ुलाम बनाने में उपयोग करने वाला एक आतंककारी समूह मजबूत हुआ, जो आज न सिर्फ़ सत्ता में है, बल्कि जो स्थितियाँ हैं, उनमें यह उत्तरोत्तर वृद्धि करते दिख रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन नई अवधारणों को विकसित करें, जो इन्हें रोकने और नई चुनौतियों के मद्देनजर बेहतर समाज के निर्माण में सक्षम हों।
लेकिन प्रगतिशील साहित्य और दलित साहित्य की असफलता के क्या कारण रहे हैं? प्रगतिशील साहित्य आन्दोलन भारतीय समाज की जाति-आधारित संरचना पर उस प्रकार चोट करने में असफल रहा है, जिस प्रकार उसके बाद आये दलित साहित्य ने की। भारतीय जाति-व्यवस्था में पिस रहे लोगों की अकांक्षाओं को नहीं समझ पाना और उसे तेवर के साथ अभिव्यक्त न कर पाना, प्रगतिशील साहित्य की मुख्य कमजोरी रही।
दलित साहित्य की अवधारणा के तहत जो लेखन हुआ उसका केंद्रबिंदु अश्पृश्यता के दंश की अभिव्यक्ति और उसका मुखर विरोध रहा। ये दोनों बहुत आवश्यक कार्यभार था, जिनमें दलित साहित्य दृढ संकल्प होकर न सिर्फ लगा रहा, बल्कि इसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। लेकिन, अनेक कारणों से यह धारा उत्तरोत्तर संकीर्ण होती हुई अनुसूचित जाति के साहित्य का पर्याय बन गयी।
दलित साहित्य की मूल चिंता अश्पृश्यता थी, इसलिए उसने इसी पर सघनता से चोट की। निरंतर संकुचन के कारण यह अवधारणा जाति-व्यवस्था से उपजे अन्य कष्टकारी स्वरूपों को अपने दायरे में लेने में विफल रही, जिससे देश के अन्य वंचित तबके, मसलन आदिवासी, घूमंतु जातियां, अन्य धर्मों के पसमांदा व हिंदुओं के अन्य अति पिछड़े वर्गों प्रभावित हैं।
इसके अतिरिक्त, इन दोनों अवधारणाओं ने विज्ञान और तकनीक के अप्रतिम फैलाव पर आलोचनात्मक नजर रखने वाली दृष्टि भी विकसित नहीं की। उनका चश्मा तकनीक के इस अप्रतिम फैलाव से पहले का है और बहुत तेजी से बदल रही दुनिया को देखने में सक्षम नहीं है।
संक्षेप में कहें तो, वाम और दलित शक्तियाँ भारतीय और वैश्विक यथार्थ की अपनी पुरानी, एकांगी समझ के कारण कमज़ोर हुईं हैं और इनके प्रभाव में सृजित साहित्य और आलाेचना की भी नये वैचारिक आलोड़न पैदा करने की क्षमता खो दी।
हम आज ऐसे समय में रह रहे हैं जब एक ओर मनुष्य और मशीन के बीच टकराहट की आशंका है तो दूसरी ओर मनुष्य और मशीन के सहअस्तित्व की संभावनाएं भी हैं। यह एक ऐसा समय है जब एक ओर ऐसा लग रहा है कि मनुष्य विज्ञान और तकनीक संबंधी अपनी उपलब्धियों के उतुंग शिखर पर पहुंचने ही वाला है और अब दुनिया की अधिकांश समस्याओं का निदान संभव होगा, तो दूसरी ओर इन उपलब्धियों पर उंगलियां पर गिने जाने वाले कॉरपोरेशनों का ऐसा कब्जा होता जा रहा है कि लगता है कि मनुष्य का इस नई गुलामी से निकलना अब असंभव होगा। तकनीक पर राज करने वाले वाले ये कॉरपोशन दुनिया की अधिकांश आबादी के मस्तिक पर कब्जा करने की क्षमता रखते हैं और इसी बूते वे विश्व के किस भी राष्ट्र-राज्य से अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं।
कोरोना वायरस महामारी की आड़ में इन बदलावों को एक ऐसी आंधी का रूप दे दिया गया, जिसमें बहुत दूर तक देख पाना कठिन हो रहा है। लेकिन, हम इतना तो देख ही सकते हैं कि मानव-सभ्यता के एक नए चरण का आगाज हो चुका है।
हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और बाजार सब बहुत तेजी से ऑनलाइन होने की प्रक्रिया में हैं।
लिखने-पढ़ने की दुनिया काफी बदल चुकी है और निकट भविष्य में इसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। मशीनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस काबिल हो चुकी है कि वह न सिर्फ स्वयं नई चीजें सीख रही है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में ऐसा बहुत कुछ पैदा करने में सक्षम हो गई है, जिन्हें कुछ वर्ष पहले तक सिर्फ मनुष्य के बूते का काम माना जाता था। हमारे देखते-देखते मशीन और मनुष्य के बीच की विभाजन-रेखा धुंधला हो रही है।
इसे एक बानगी से समझें, मशीनों के इस नए अवतार के कारण दुनिया की प्रतिष्ठित विज्ञान विषयों की शोध पत्रिकाएं एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही हैं। इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर लेखकों को उनकी नौकरियों में प्रमोशन, आर्थिक अनुदान आदि अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अनेक लेखक इन पत्रिकाओं को प्रकाशनार्थ मशीनों द्वारा तैयार किए गए फर्जी शोध-पत्र भेज रहे हैं। मशीनों द्वारा इंटरनेट पर मौजूद वैज्ञानिक शोधों के अथाह सागर से एकदम मौजूं संदर्भ ढूंढ कर सजाए गए ये ‘शोध-पत्र’ बिल्कुल मौलिक जैसे लगते हैं। पीयर रिव्यू करने वाले ऐसे जाली शोध-पत्रों को पकड़ पाने में असफल हो रहे हैं।
फर्जी शोध-पत्रों की बात छोड़ भी दें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उन्नत प्रणालियां जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायनशास्त्र में नित नई-नई अत्यंत उपयोगी खोजें कर रही हैं। महामारी के वर्षों के दौरान ही अल्फाफोल्ड नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी सफलता हासिल की, जिसने चिकित्साशास्त्र को युगांतकारी छलांग दे दी है। इस खोज के कारण अब यह पता लगाना संभव हो गया है कि अमीनो एसिड की एक शृंखला कैसे थ्री-डी आकार में परिवर्तित होकर जीवन के कार्यों को अंजाम देती है। इससे अब पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले मनुष्य समेत 10 लाख जीवों और सभी वनस्पतियों में मौजूद 20 करोड़ से अधिक प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी संभव हो गई है, जो नई दवाओं और टीका के निर्माण में सहयोगी हो रही है।
यह अनायास ही नहीं कहा जा रहा कि मशीनें जिस तेज गति से चिकित्सा विज्ञान में नई-नई खोजें करने में सफल हो रही हैं, उससे संभावना है कि, अगर नोबल देने का मौजूदा पैमाना बरकरार रहा तो वर्ष 2036 तक नोबेल पुरस्कार किसी मशीन को देना होगा।
यह सब सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लेखन, चित्रकला, संगीत के क्षेत्र में भी मशीनें तेजी से पैठ बना रही हैं। अब वे संगीत की नई धुनें स्वयं बना ले रही हैं, ऐसी पेंटिंग्स कर रही हैं, जिनमें अर्थवत्ता समेत प्राय: ऐसा बहुत कुछ है, जो किसी बड़े चित्रकार के चित्र में पाया जाता था। पत्रकारिता में भी उसके कदम पड़ चुके हैं। दुनिया के बड़े मीडिया संस्थान मशीनों से डेस्क-संवाददता का काम लेना शुरू कर चुके हैं। अनेक सर्वेक्षणों में पाया गया कि मशीनों द्वारा लिखे गए खेल व आर्थिक विषयों से संबंधित समाचार मनुष्य संवाददाताओं की तुलना में किंचित गहरे और प्रभावशाली हैं।
मानविकी से संबंधित अकादमिक अनुशासनों में भी इसका पदापर्ण हो चुका है। डिजिटल ह्यूमैनिटिज नामक एक नया अनुशासन पिछले वर्षों में बना और विकसित हुआ है, जिसके सहारे अब हम साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल समेत सभी मानविकी अनुशासनों में ऐसी अनूठी चीजें पलक झपकते देखने में सक्षम हो रहे हैं, जिनके बारे में पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मशीनें कविताएं और उपन्यास भी लिख रही हैं, और पाठक के लिए पकड़ पाना संभव नहीं रह गया है कि उसका कौन सा हिस्सा मशीन द्वारा लिखा गया है और किस हिस्से को किसी मनुष्य की रचनात्मकता ने संवारा है। औद्योगिक क्रांति के समय मशीनें मनुष्य के शारीरिक श्रम में सहयोगी के रूप में सामने आईं थी, अब वे हमारी बौद्धिक और रचनाशील सहकर्मी की भूमिका में आने को आतुर हैं। स्वाभाविक तौर पर इन परिवर्तनों से, विचार और दर्शन की दुनिया भी बदल रही है। इसका दायरा मनुष्योन्मुखी संकीर्णता का त्याग कर समस्त जीव-जंतुओं और बनस्पितयों तक फैल रहा है। एंथ्रोपोसीन और उत्तर मानववाद जैसी विचार-सरणियों के तहत इनपर जोरशोर से विमर्श हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज इनसे अछूता है। युवा पाठक आज आधिकांश मायनों में अपने लेखकों से बहुत आगे है। नित तेज होते बैंडबिथ पर वह सूचनाओं और ज्ञान की वैश्विक दुनिया की झलकियां देख रहा है। मशीनी अनुवाद की सफलता से भाषा के बंधन भी तेजी से टूट रहे हैं।
हमें इन परिवर्तनों को एक आसन्न संकट की तरह नहीं, बल्कि परिवर्तन की अवश्यंभावी प्रक्रिया के रूप लेना चाहिए और इसके उद्देश्यों की वैधता पर पैनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के साहित्य और वैचारिकी में इसकी गूंज सुनाई नहीं पड़ रही।
इन चीजों का विश्लेषण और प्रतिरोध का उपकरण न प्रगतिशील साहित्य के पास है, न ही दलित साहित्य के पास। उनके उपकरण यह चिन्हित ही नहीं कर पाते कि विज्ञान और तकनीक किस सीमा पर पहुंच कर निरपेक्ष नहीं रह जाते। प्रगतिशील आंदोलन अभी भी अपना पुराना परचम लहराते हुए पूंजीवाद का पुराने पड़ चुके तरीकों से विरोध करने में जुटा है, जबकि दलित अवधारणा विज्ञान और तकनीक का इस प्रकार जयघोष करने में लगी है, मानो ब्राह्मणवादियों ने विज्ञान और तकनीक के विकास और उसकी उपलब्धता को रोक रखा हो, और यह रोक हटते ही अधिकांश समस्याओं का हल हो जाएगा।
ऐसे अनेक कारणों से एक नई अवधारणा की ज़रूरत महसूस होने लगी है।
लेकिन अभी इसके तहत मुख्य रूप से भारतीय समाज के विभिन्न वंचित-शोषित सामाजिक तबकों और कम्युनिस्ट मिजाज के लोगोंं की एकता और मुद्दों के साझेपन की बातें ही की जा रही हैं। हालाँकि साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में इसके मायने अधिक जटिल, सूक्ष्म और दूरगामी हैं और होने चाहिए।
बहुजन अवधारणा के विरोध में कौन है?
बहरहाल, कौन-सी शक्तियाँ इस अवधारणा के पक्ष में हैं या हो सकते हैं, यह तो स्पष्ट ही है। लेकिन अगर हम यह ग़ौर करें कि कौन-सी शक्तियाँ इस अवधारणा से सबसे अधिक विचलित हैं, तो इसकी ताक़त का बेहतर अनुमान हो सकता है।
सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर बहुजन अवधारणा की सैद्धांतिकी के निर्माण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध पत्र पाञ्चजन्य और आर्गेनाइजर ने सबसे पहले सुनियोजित रूप से हमला किया, जो निरंतर जारी है। उनका यह विरोध चलताऊ क़िस्म का नहीं है, बल्कि वे इसके विरोध में अपनी विचारधारा के आधार पर एक सैद्धांतिकी गढ़ने की कोशिश करते हैं। मसलन, बहुजन अवधारणा का उल्लेख करते हुए पाञ्चजन्य कहता है कि ये लोग ‘भारतीय संविधान व राज-व्यवस्था द्वारा नागरिक-अधिकारों के संरक्षण हेतु सृजित कोटियों (यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) को अपरिवर्तनीय एवं परस्पर संघर्षरत नस्ली समूहों में रूढ़’ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ग़ौर करने लायक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक अस्तित्व के रूढ़ बने रहने से न सिर्फ़ सहमत हैं, बल्कि इसे अपने कथित ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ और ‘हिंदुत्व’ के लिए हितकर मानता है। इसके विपरीत इन तबक़ों के सांस्कृतिक और साहित्यिक साझेपन को रेखांकित किये जाने को कथित हिन्दुत्व, जो कि वास्तव में द्विजवाद का मुखौटा है; के लिए विकट ख़तरे के रूप में देखता। बहुजन अवधारणा को राष्ट्रवाद के विरोध में बताने वाली ऐसी अनेक सामग्री पाञ्चजन्य और आर्गेनाइजर में प्रकाशित हुई हैं।
वस्तुत: बहुजन अवधारणा इन सामाजिक श्रेणियों को रूढ़ नहीं बनाती, बल्कि इन्हें श्रेणीक्रमों से मुक्त करती है और इस प्रकार प्रकारांतर से जाति मुक्ति की ओर बढ़ती है। यह मानवीय गरिमा और मानव-स्वातंत्र्य को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक रूप से समतामूलक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह अवधारणा कहती है कि ‘सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों में पैदा हुए लोग, जिन्हें हम आम बोलचाल में सवर्ण कहते हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं, जिनके पारिवारिक संस्कार और बौद्धिक प्रतिबद्धताएँ निरंतर धींगामुश्ती कर रही होती हैं। उन्हें साहित्य ने, समाज ने, विज्ञान ने, इतिहास ने जो जानकारियाँ और सबक़ दिये हैं, वे उन्हें बेचैन किये हैं कि कहीं वे उल्टी दिशा में तो नहीं खड़े हैं।’ बहुजन अवधारणा सामाजिक समानता के पक्षधर इन लोगों को भी स्वयं में समाहित करती है।
इस प्रकार, यह जड़ अस्मितावाद की अवधारणा नहीं है, बल्कि इसे दुनिया आज जिन समस्याओं से आज जूझ रही है, उसे समझने और उनसे निजात पाने की बौद्धिक परियोजना के रूप में विकसित हो रही है। अभी शुरूआत है, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद यह इसी दिशा में पल्लवित होगी।
बहुजन साहित्य का इतिहास
साहित्य में बहुजन अवधारणा को प्रबल बनाने की कोशिशों का इतिहास लम्बा है। इसके नामाकरण में बुद्ध की उक्ति ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ की दार्शनिक प्रेरणा है। हिन्दी में भिक्खु बोधानंद (1874-1952), स्वामी अछूतानंद (1879-1933), चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु (1885-1974) आदि ने इस अवधारणा को लेकर विपुल लेखन किया। इन लोगों ने इस अवधारणा के प्रसार के लिए प्रकाशन गृह चलाये तथा अनेकानेक पुस्तकें प्रकाशित कीं, सैकड़ों सभाएं और गोष्ठियां कीं। उत्तर भारत में त्रिवेणी संघ, (1930 के आसपास निर्मित) अर्जक संघ (1968 में स्थापित) जैसे अनेक मज़बूत सामाजिक-राजनीतिक संगठन भी इस विचारधारा को केंद्र में रखकर ही सक्रिय रहे। दक्षिण भारत में रामासामी पेरियार (1879-1973) आन्दोलन की धुरी भी बहुजन अवधारणा ही थी। महराष्ट्र में जोतीराव फुले (1827-1890) ने भी जो आन्दोलन खड़ा किया, वह दलित या पिछड़ा आन्दोलन नहीं था, बल्कि बहुजन आन्दोलन ही था। उन्होंने ‘शूद्रों और अतिशूद्रों’ की एकता की बात की और इनके साझेपन का सांस्कृतिक आधार तैयार करने के लिए विपुल लेखन किया। बहुजन अवधारणा पर काम करने वाले इन लेखकों और समाज सुधारकों का मुख्य कार्यभार सामाजिक संकीर्णताओं और वर्चस्ववाद से मानव-जीवन को मुक्त करना और सामाजिक समता काे विकसित करने वाली आध्यत्मिकता का विकास करना था।
बहुजन अवधारणा की इस धारा को किस प्रकार परवर्ती राजनेताओं और बौद्धिकों ने जाने-अनजाने संकीर्ण बनाया, उस पर अन्यत्र लिख चुका हूँ। (देखें, ‘हिंदी साहित्येतिहास का बहुजन पक्ष’, अनन्य प्रकाशन, 2016 तथा मेरा लेख ‘त्रिवेणी संघ का साहित्य और साहित्य में त्रिवेणी संघ’)
बहरहाल, बहुजन साहित्य की अवधारणा के मौज़ूदा दौर का आरम्भ वर्ष 2011 के इर्द-गिर्द होता दिखता है। उस समय मैंने फारवर्ड प्रेस नामक मासिक पत्रिका में इसके सैद्धांतिक पक्ष को विकसित करने वाले लेख प्रकाशित करना आरम्भ किया तथा हर वर्ष अप्रैल में, जो कि फुले-आम्बेडकर के जन्मदिन का माह है; उस पत्रिका की ‘बहुजन साहित्य वार्षिकी’ का प्रकाशन किया। ऐसी पाँच वार्षिकियाँ प्रकाशित हुईं, जिनमें इस अवधारणा के संदर्भ में हिन्दी के अधिकांश महत्त्वपूर्ण लेखकों के विचार सामने लाये गये। इस क्रम में कुछ किन्तु-परन्तु के साथ लगभग सभी लेखक इस अवधारणा की आवश्यकता से सहमत थे। उन अंकों में अधिकांश लेखकों ने इसकी मूल्य-संहिता और साैंदर्य-शास्त्र को लोगों के सामने रखने की आवश्यकता पर बल दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें अब समय के साथ-साथ पल्लवित हो रहीं हैं, लेकिन इनके सैद्धांतिकरण की आवश्यकता तो है ही।
बहुजन साहित्य की सैद्धांतिकी
भारतीय संदर्भ में बहुजन अवधारणा अपना मुख्य ताना-बाना सिर्फ आर्थिक मुद्दों के इर्द-गिर्द न बुनकर, भारतीय जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता से उत्पन्न समस्याओं को केंद्र में रखती है। यह अवधारणा मानती है कि आर्थिक समानता की दिशा की मूल बाधा में हमारी सामाजिक-व्यवस्था है। यही कारण है कि यह अवधारणा सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को शीर्ष पर रखती है और विज्ञान और तकनीक की प्रगति की दिशा का अपनी वैचारिकी के आधार पर आलोचनात्मक मूल्यांकन पर बल देती है।
साहित्य, विशेषकर आलोचना में इस अवधारणा को सामने रखते ही भारतीय वर्ण-व्यवस्था के ऐसे अनेक पहलू सामने आने लगते हैं, जिनकी ओर दलित और मार्क्सवादी धाराओं के सहारे हम नहीं देख पा रहे थे। मसलन, उपरोक्त अवधाराणाओं में शिल्पकार और किसान जातियों की पीड़ा और इनके अलग हितों को या तो ओझल कर दिया जाता है, या फिर इन सबको एक ही डण्डे से हाँकते हुए सामाजिक रूप से शोषक या पूँजीवाद का पिछलग्गू करार दिया जाता है। इन अवधारणाओं में अति-पिछड़े हिन्दू समुदायों, पसमांदा मुसलमानों, घुमंतू जातियों, अन्य धर्मांतरित समुदायों पर अलग से नज़र डालने की ज़रूरत तक नहीं समझी जाती। आदिवासियों और स्त्रियों की अभिव्यक्तियों को एकदम अलग-थलग कर दिया जाता है।
जबकि बहुजन अवधारणा को सामने रखने पर हम इन समुदायों की पीड़ा, शोषण और साहित्यिक-अभिव्यक्तियों की समानताओं को आसानी से देख पाते हैं। जैसे-जैसे यह अवधारणा पल्लवित हो रही है, इन समुदायों की संस्कृति और उनके वैचारिक आधारों की एकता भी दिखने लगी है। इसके अतिरिक्त बहुजन अवधारणा ब्राह्मणवाद के स्थान पर अभिजनवाद को रखती है, जो सामाजिक रूप से ‘द्विजवाद’ के क़रीब है। इस प्रकार यह अपनी विरोधी शक्तियों और उनकी नित बदलती रणनीतियों को भी अधिक सघनता से चिह्नित करने और उनका विरोध करने में सक्षम हो जाती है। लेकिन, जैसा कि मैंने पहले संकेत किया, बहुजन साहित्य की अवधारणा अस्मितावादी नहीं है। यह ‘बहुसंख्यकों के कल्याण’ पर आधारित है, लेकिन यह ‘बहुसंख्यकवाद’ नहीं है। इस फर्क को गहराई से रेखांकित किए जाने की जरूरत है। यह ‘बहु-मत’ को नहीं, बहुसंख्यकों के वास्तविक हित को ध्यान में रखती है।
इस अवधारणा में लेखक की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन तो जारी रहता है, लेकिन जैसा कि प्रेमकुमार मणि ने कहते हैं, इसमें “लेखक का दृष्टिकोण क्या है, यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।” यह ‘जाति’ पर नहीं, ‘जन’ पर केंद्रित विचारधारा है। यह ‘जाति से जमात’ की ओर की यात्रा नहीं है, बल्कि जाति मात्र से मुक्ति की, एक सुंदर सामाजिक जीवन और श्रमण परंपरा में मौजूद आध्यात्म के विकास की परिकल्पना है, जिसके मूल में वैज्ञानिकता का वास है।
इन अवधारणा के आरंभिक दार्शनिकों (कौत्स, बुद्ध, मक्खली गोशाल, अजित केशकंबली आदि) के दर्शन की मूल बिंदू अपने समय में शाश्वत सत्य के रूप में प्रचारित की गई मिथ्या विचाराधाराओं को चुनौती देना तथा बहु-जनों का कल्याण करने वाली विचारधारा का निर्माण करना रहा है। इन दार्शनिकों ने सिर्फ तात्कालिक समस्याओं पर ही नजर नहीं रखी, बल्कि पूरी प्रकृति को स्वयं में समेटने वाली आध्यात्मिकता का प्रस्ताव किया। इसलिए इस अवधारणा के तहत लेखन करने वालों के लिए विज्ञान और तकनीक के विकास पर आलोचनात्मक नज़र बनाये रखना भी आवश्यक हो जाता है; क्योंकि इसका एक मुख्य कार्यभार बहुजनों की दूरगामी हित और उनकी खुशी है, न कि कथित ‘विकास’, जिसके नाम पर विशाल कॉरपोरेशन दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों को बंधुआ बनाते जा रहे हैं।
अन्य चीज़ों के अतिरिक्त ‘बहुजन साहित्य की अवधारणा’ जिस चेतना को प्रसारित करती है, वह चेतना मनुष्य और प्रकृति के ऐतिहासिक सह-अस्तित्व को स्वीकार करने वाले तथा मानवीय श्रम को गरिमा देने वाले लेखन को श्रेयस्कर मानती है।
बहुजन साहित्य का अर्थ है– अभिजन के विपरीत बहुजन का साहित्य और उनकी वैचारिकी। प्रगतिशील- मार्क्सवादी विचारधारा में जो ‘जन’ है, ‘बहुजन’ उसकी अगली कड़ी भी है। मार्क्सवाद के ‘जन’ का अर्थ भारत के सामाजिक-यथार्थ के संदर्भ में न सिर्फ अस्पष्ट और अनिश्चित बना रहता है, बल्कि वह हमारे सांस्कृतिक मंतव्यों को प्रकट नहीं करता। जब हम ‘जन’ में ‘बहु’ प्रत्यय जोड़ते हैं तो इससे बना शब्द हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में वैचारिक और दार्शनिक रूप से भी जीवंत बन उठता है। यह हमें भारत की श्रमणवादी धारा के दार्शनिकों, कौत्स, बुद्ध, मक्खली गोशाल, अजित केशकंबली आदि की वैज्ञानिक चेतना से जोड़ देता है और उनके दर्शन को समकालीन आवश्यकता के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। “बहुजन” में बहुलता का भाव है। नए भाषा संकेतों का सहारा लेकर कहें तो यह जन + (जन प्लस) भी है। जन+ के अर्थ में यह पिछले दो दशक से पश्चिम में चर्चित हो रही उत्तर-मानववाद जैसी धारणााओं को तार्किक दिशा देने में भी सक्षम है। थोड़ा वक्रोक्ति का प्रयोग करते हुए कहें तो “प्रगतिशील साहित्य में वंचित तबकों के दु:खों का चित्रण तो हुआ, लेकिन वह उन दाहक दु:खों के कारण के रूप में ब्राह्मणवाद को चिन्हित में सक्षम नहीं था। दलित साहित्य को दु:ख देने वाला भी दिखा, उसने उन दु:खों के कारणों को गहराई से रेखांकित किया। बहुजन साहित्य की अवधारणा से दु:ख भी दिखता है, दु:ख देने वाला भी दिखता है, और दुख से मुक्ति का उपाय भी दिखता है।
इस अवधारणा को केंद्र में रखकर अधिकाधिक आलोचना-कर्म करने की ज़रूरत है, ताकि इसके मूल्य और अधिक निखरकर सामने आएँ।
(प्रमोद रंजन की दिलचस्पी सबाल्टर्न अध्ययन, आधुनिकता के विकास और ज्ञान के दर्शन में रही है। ‘साहित्येतिहास का बहुजन पक्ष’, ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ और ‘शिमला-डायरी’ उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं।)
संपर्क : हिंदी विभाग, असम विश्वविद्यालय, दीफू परिसर, दीफू, असम, पिन कोड : 782462, Mo : 9811884495